इतिहास, संस्कृति और संविधान: भारत की पहचान का संगम
शोध सारांश जमा करने की अंतिम तिथि बढ़कर 15 अक्टूबर हुई, इतिहास और संस्कृति में निहित है भारतीय संविधान की आत्मा।
- भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप संविधान के हर पहलू में देखी जा सकती है।
- संविधान में न्याय, समानता और लोककल्याण के सिद्धांत भारत की प्राचीन शासन पद्धतियों से प्रेरित हैं।
- शोधकर्ताओं के लिए शोध सारांश जमा करने की अंतिम तिथि अब 15 अक्टूबर कर दी गई है।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2025: भारत का संविधान केवल एक आधुनिक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जड़ें देश के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में गहरी समाई हुई हैं। इस विषय पर शोध कर रहे विद्वानों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है: शोध सारांश जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, जो अब 15 अक्टूबर है। यह विस्तार उन सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और संविधान के अंतर्संबंधों पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं।

भारत का इतिहास सिर्फ राजवंशों और लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाहित होने वाली सांस्कृतिक धारा है जिसने समाज को आकार दिया है। यह ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक अनुभव हमारे संविधान के निर्माण में भी प्रतिबिंबित होते हैं। उदाहरण के लिए, मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्यों की शासन पद्धतियों का मूल आधार न्याय और प्रजा-हित था। सम्राट अशोक के शिलालेखों में धर्म, सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों पर आधारित शासन की जो झलक मिलती है, वही भावना हमें संविधान के धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में दिखाई देती है।

विविधता में एकता का सांस्कृतिक आदर्श
भारतीय संस्कृति ने सदैव ही विविधता और सहिष्णुता का आदर्श स्थापित किया है। वैदिक युग से लेकर उपनिषद, बौद्ध और जैन दर्शन, भक्ति आंदोलन के संतों और सूफी परंपराओं तक, सभी ने एक ऐसी बहुलतावादी और उदार समाज की नींव रखी जिसने भारतीय समाज को एक साथ जोड़ा। संविधान निर्माताओं ने इसी बहुलतावादी संस्कृति का सम्मान करते हुए लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों को अपनाया। यह भारतीय संतों की परंपरा थी जिसने सामाजिक न्याय की प्रेरणा दी, गंगा-जमुनी तहजीब ने धर्मनिरपेक्षता को आधार दिया और प्रजा-हितकारी शासकों की परंपरा ने एक कल्याणकारी राज्य की धारणा को जन्म दिया।

संविधान सभा के कार्य में भी यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना स्पष्ट रूप से मौजूद थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को संविधान की आत्मा माना, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिकता और लोकतांत्रिक परंपरा के बीच संतुलन साधा। सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत की विविध रियासतों और संस्कृतियों को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को संविधान में स्थान देने पर जोर दिया।

नागरिकों के कर्तव्यों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिबिंब
भारतीय संविधान केवल नागरिकों के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि उनके कर्तव्यों को भी महत्व देता है। संविधान का अनुच्छेद 51(क) नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है, जिसमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और राष्ट्रीय एकता का बोध शामिल है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, संविधान का पालन करना और हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना, ये सभी कर्तव्य सीधे तौर पर भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं।
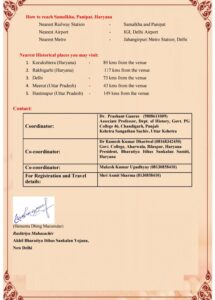
इस तरह, भारतीय इतिहास, संस्कृति और संविधान एक-दूसरे के पूरक हैं। संविधान ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भारतीय परंपराओं को भी मजबूत किया है। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की आत्मा का दर्पण है, जो उसके संघर्षों और आदर्शों को दर्शाता है। भारतीय संविधान को पूरी तरह से समझना तभी संभव है जब हम इसे इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखें।
लेटेस्ट हिंदी समाचार अपडेट के लिए Facebook पर Samagra Bharat के पेज को फॉलो करें।

